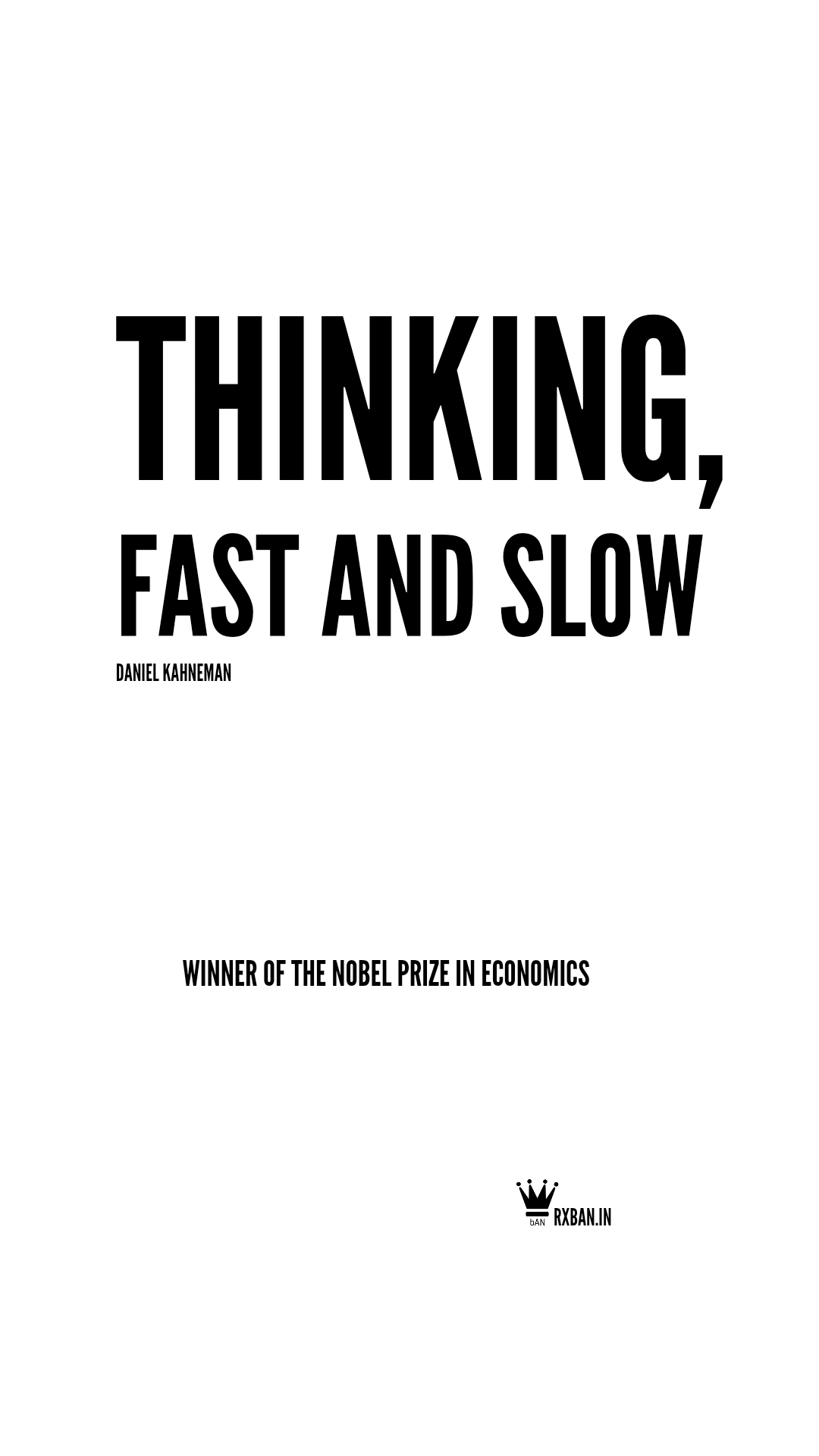Thinking Fast and Slow

Cool बनने की कोशिश में fool बनता हुआ दिमाग
दिमाग हमेशा एक पहेली की तरह रहा है। साल 2011 में आई ये किताब इसे थोड़ा सुलझाने में आपकी मदद करती है। डेनियल को उनकी इस रिसर्च के लिए नोबेल दिया जा चुका है जहां उन्होंने साइकोलॉजी और इकॉनमिक्स के कनेक्शन को समझाने पर काम किया था। ये किताब इसकी एक झलक आप तक लाती है। इन सालों में इस रिसर्च ने दिमाग और हमारे बर्ताव को समझने के लिए दूसरे रिसर्चर्स की भी बहुत मदद की है। इसे पढ़कर आपको ये भी पता चलता है कि कुछ गल्तियां इतनी कॉमन क्यों हैं और हम इनसे किस तरह बच सकते हैं।
लेखक
Daniel Kahneman को साल 2002 में इकॉनमिक्स के लिए नोबेल दिया गया था। वो Woodrow Wilson School of Public and International Affairs और Center for Rationality at the Hebrew University in Jerusalem के फैलो और Princeton University में साइकोलॉजी के Eugene Higgins Professor के तौर पर जुड़े हुए हैं।
The lazy mind: आलस किस तरह हमारे दिमाग पर असर डालता है?
हम अक्सर सुनते हैं कि ये काम सोच समझकर किया गया और वो एकदम ऑटोमेटिक तरीके से। यानि हमारे बर्ताव को इन दो तरह से बांटा जा सकता है automatic और considered लेकिन दिमाग के अंदर इन दो तरीकों को लेकर जैसे कोई फिल्मी ड्रामा चल रहा होता है जहां दो हीरो एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं। एक है impulsive, automatic, intuitive यानि System 1 और दूसरा है thoughtful, deliberate, calculating यानि System 2 और इनके आमने सामने आने से ये तय होता है कि हमारा अगला कदम क्या होगा, हम कैसे सोचेंगे और कैसे कोई फैसला करेंगे। System 1 हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो intuitively और एक झटके में काम करता है। अक्सर इस तरह जहां हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं रहता। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक तेज आवाज आती है। आप क्या करेंगे? तुरंत पलटकर देखेंगे ना। System 1 यही है। हमारे इवॉल्यूशन के इतिहास में ये सिस्टम काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि सर्वाइवल के लिए यही सिस्टम काम आता रहा है। यानि कोई खतरा दिखा तो तुरंत फैसला लेकर एक्ट करना।
System 2 वो हिस्सा है जहां decision-making, reasoning और beliefs काम पर लगे होते हैं। इसमें दिमाग की सारी conscious activities जैसे कि self-control, choices, focus और attention शामिल हैं। जैसे मान लीजिए आप भीड़ में किसी महिला को ढूंढ रहे हैं यानि आपका दिमाग deliberately एक ही काम पर फोकस करेगा। अब आप बार बार वही चीज देखेंगे जो उस महिला से जुड़ी हों या उसे देखने में मदद करें। इस फोकस की वजह से आपका ध्यान नहीं भटकता और आप शायद ही भीड़ में खड़े किसी और इंसान पर ध्यान देते हैं। अगर आपका फोकस ऐसे ही बना रहा तो आप मिनटों में उसको ढूंढ निकालेंगे जबकि ध्यान भटक गया तो आपको घंटों लग सकते हैं। आगे देखते हैं कि इन सिस्टम की वजह से हमारे बर्ताव पर क्या असर पड़ता है।
इन दोनों सिस्टम के काम के तरीके को समझने के लिए जानी मानी bat-and-ball पहेली को हल करते हैं। एक बैट और बॉल की कीमत है 110 रुपए। बैट की कीमत बॉल से 100 रुपए ज्यादा है। तो बॉल कितने की होगी? इस बात की काफी संभावना है कि आप बोल दें दस रुपए। इसकी वजह है आपका intuitive और automatic System 1 जबकि ये जवाब गलत है। अब आराम से हिसाब लगाकर देखिए। बॉल की असली कीमत है 5 रुपए। अब देखिए कि जब सिस्टम 1 ने चार्ज लेकर ऑटोमेटिक तरीके से जवाब दिया तो जवाब गलत था लेकिन जवाब आया बहुत जल्दी। लेकिन सिस्टम 1 ऐसी किसी सिचुएशन में फंसने पर सिस्टम 2 को आवाज लगाता है। लेकिन इस बैट बॉल की पहेली में सिस्टम 1 धोखा खा गया। उसे लगा कि ये तो बहुत आसान सवाल है जिसे मैं खुद हैंडल कर सकता हूं। लेकिन ये बैट बॉल की पहेली हमारे पैदाइशी दिमागी आलस की तरफ इशारा करती है। जब कभी हम दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर काम में कम से कम एनर्जी खर्च हो। इसे law of least effort के नाम से जाना जाता है। अब सिस्टम 2 की मदद लेकर जवाब ढूंढना ज्यादा एनर्जी लगाने वाला काम था तो हमारे दिमाग ने ये सोचकर कि ये तो आसान सा सवाल है वो एनर्जी बचा ली। हालांकि ये आलस हमारा ही नुकसान करता है क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस के लिए सिस्टम 2 एक बहुत जरूरी हिस्सा है। रिसर्च बताती हैं कि सिस्टम 2 वाली एक्टिविटीज जैसे फोकस और सेल्फ कंट्रोल की मदद से हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। अगर इस पहेली को सुलझाते हुए भी सिस्टम 2 की मदद ली जाती तो नतीजा कुछ और निकलता पर आलस ने सिस्टम 2 को नजरअंदाज कर दिया और इंटेलिजेंस को भी आगे बढ़ने नहीं दिया।
Autopilot: हम ऑटो पायलट मोड में क्यों जाते हैं?
अच्छा अगर कभी आपको ये शब्द “SO_P” दिखाया जाए तो आप खाली जगह पर क्या भरेंगे? चलो मान लिया आपके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। पर आपको ये कहा जाए कि ये खानपान से जुड़ी चीज है तो? अब शायद आप इसे “SOUP” लिखकर पूरा कर दें। इस प्रोसेस को priming कहते हैं। हम ऐसी हर सिचुएशन के लिए primed होते हैं। यानि कोई शब्द, मौका या बात जो हमें किसी दूसरे मौके या शब्द से जोड़ दे। अगर आपसे ये कहा जाता कि ये शब्द नहाने से जुड़ा है तो आप “SOAP” लिखकर खाली जगह भर देते। ये priming हमारी सोच ही नहीं बल्कि एक्शन पर भी असर डालती है। Priming का असर दिमाग ही नहीं शरीर पर भी पड़ता है। इस पर एक स्टडी की गई। जब इसमें भाग लेने वालों को ऐसे शब्द बोले गए जो बढ़ती उम्र से जुड़े थे जैसे झुर्रियां तो उन्होंने धीरे चलना शुरू कर दिया। अब मजे की बात ये है कि priming बिल्कुल unconscious होती है। यानि हम सोचे समझे बिना ही ऐसा करने लगते हैं।
हमें priming से ये बात समझ आती है कि चाहे हम कितने ही दावे कर लें पर हमेशा सोच समझकर फैसले या एक्ट करना हमारे बस में नहीं है। हम किसी ना किसी सोशल या कल्चरल priming के असर में रहते ही हैं। जैसे Kathleen Vohs की एक रिसर्च से ये साबित हुआ कि पैसा भी priming के लिए जिम्मेदार होता है। यानि पैसा हमको self centered बनाता है। लोग पैसे से पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। अगर पैसों की इमेज भी दिखाई जाती रहे तो लोग अपने फायदे के लिए ज्यादा सोचते हैं और दूसरों की सलाह, बातें या उनकी जरूरत को नजरअंदाज करते जाते हैं। इस रिसर्च का एक पहलू ये भी है कि पैसों से प्रभावित हो जाने वाले समाज में रहकर हम दया और करुणा जैसी बातों से दूर हो जाते हैं। दूसरी किसी भी सोशल चीज की तरह priming भी हमारी सोच और फिर चॉइस, जजमेंट और बर्ताव पर असर डाल सकती है। ये सब उस समाज को बनाने में मदद करते हैं जिसका हम हिस्सा हैं।
Snap judgments: आखिर हमारा दिमाग बिना सोचे समझे फैसले लेता कैसे है?
मान लीजिए आपको पार्टी में कोई मिला जिससे बातचीत करके आपको अच्छा लगा। अब किसी दिन कोई आपसे पूछता है कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो सोशल एक्टिविटी में हाथ बंटा सके और आपको तुरंत उसी इंसान का ख्याल आ जाता है। लेकिन आप उसके बारे में जानते ही क्या हैं? आपने तो बस एक बार उससे मुलाकात ही की थी। असल में आपको उसकी कोई एक बात अच्छी लगी और आपने ये सोच लिया कि आपको उसकी हर बात अच्छी लगेगी। हम भले ही किसी के बारे में ज्यादा ना जानते हों पर उसे अच्छा या बुरा ठहराने में देर नहीं करते। लेकिन बिना कुछ जाने समझे इतनी आसानी से कोई राय बना लेने से अक्सर फैसले लेने में गल्ती हो जाती है। इसे exaggerated emotional coherence या फिर halo effect कहा जाता है। यानि उस इंसान के बारे में कुछ अच्छा लगा और आपने उसके चारों तरफ एक halo बना दिया। लेकिन दिमाग और भी ढेर सारे शॉर्टकट बनाता है। इसमें काफी bias भी शामिल हैं। यानि लोग अक्सर किसी चीज के बारे में सुनी सुनाई बातों पर अपनी राय बना लेते हैं और आगे भी वही बात सच मानते हैं जो उनकी पहले से बनी सोच के मुताबिक हो। जैसे ये सोचना कि सिगरेट पीने वाले बुरे होते हैं।
अब अगर कोई आपसे किसी सिगरेट पीने वाले इंसान के बारे में पूछे जिसको आप ज्यादा ना भी जानते हों तो भी आपका जवाब उसे लेकर कुछ खास अच्छा नहीं होगा। ये halo effect और confirmation bias होते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारा दिमाग जल्दबाजी करता है। लेकिन इससे गल्तियां होने लगती हैं क्योंकि हमारे पास सही गलत का हिसाब लगाने के लिए पूरी जानकारी ही नहीं होती। हमारा दिमाग आधी अधूरी जानकारी या कामचलाऊ तरीकों से बात पूरी करने में लगा रहता है। यानि priming की तरह ये cognitive phenomena भी हमारी conscious awareness के बिना होता है और हमारे एक्शन और फैसलों पर असर डालता है।
Heuristics: शॉर्टकट के तरीके
हम अक्सर खुद को ऐसी किसी ना किसी सिचुएशन में पाते हैं जहां हमें जल्दी फैसले लेने होते हैं। इसके लिए हमारे दिमाग ने कुछ ऐसे शॉर्टकट ढूंढ लिए हैं जो हमें ऐसी सिचुएशन को तुरंत समझ पाने में मदद करें। इनको heuristics कहा जाता है। ये तरीके ज्यादातर हमारे लिए फायदेमंद ही होते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि हमारा दिमाग इनको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है। ऐसी सिचुएशन में भी इनका सहारा लेना जहां इनका रोल नहीं है गल्ती की वजह बन सकता है। ये heuristic वैसे तो बहुत से होते हैं पर इनको और अच्छी तरह समझने के लिए हम इनके दो टाइप समझते हैं। इनके नाम हैं substitution heuristic और availability heuristic. अब substitution heuristic का मतलब है कि जो सवाल पूछा गया है हम उसकी जगह उससे मिलता जुलता आसान सवाल बनाकर जवाब दें। जैसे एक लॉ फर्म में कोई वकील की नौकरी के लिए आता है। आपसे उसके बारे में राय पूछी जाती है जबकि आपको कुछ पता नहीं है। यहां आप ये कह देंगे कि क्या वो अच्छे वकील की तरह लगता है?
यानि बजाए उसकी स्किल या नॉलेज समझे बिना अपने मन में पहले से बनी किसी वकील की इमेज पर उसके खरे उतरने या ना उतरने पर बात चली जाती है। अगर इंटरव्यू देने वाला इमेज पर खरा ना उतरे तो हम उसे ना कह देंगे भले ही उसे कितनी नॉलेज या एक्सपीरियंस क्यों ना हो या वो सबसे बेहतरीन कैंडीडेट हो। अब बात करते हैं availability heuristic की। इसका मतलब है किसी चीज के होने की संभावना को बढ़ाकर मान लेना क्योंकि आप लगातार उसके बारे में सुनते रहते हैं या वो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाती है। जैसे अगर हम डेटा देखें तो एक्सीडेंट से ज्यादा लोग स्ट्रोक से मरते हैं। पर जब एक स्टडी में लोगों से यही सवाल पूछा गया तो 80% ने एक्सीडेंट को ऊपर रखा। इसकि वजह ये थी कि हम रोज एक्सीडेंट की खबरें पढ़ते सुनते रहते हैं और ऐसे किसी बुरे हादसे की खबर स्ट्रोक की खबर से ज्यादा आसानी से याद रखते हैं। हो सकता है इस वजह से हम स्ट्रोक के खतरे को नजरअंदाज भी कर दें।
No head for numbers: नंबरों से होने वाली गल्तियां
आप किसी चीज के होने का अंदाजा कैसे लगाते हैं? जवाब है डेटा से। जैसे कोई बड़ी टैक्सी कंपनी है जहां 20% पीली कारें हैं और 80% लाल। इसका मतलब ये भी है कि पीली कारों की हायरिंग 20% और लाल कारों की हायरिंग 80% हो सकती है। अब आपको कोई कैब हायर करके इसके रंग का अंदाजा लगाना है तो आपको ये डेटा याद रखना होगा। आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। हम अक्सर ऐसे डेटा भूल या नजरअंदाज कर जाते हैं। इसकी एक वजह ये है कि हम उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हों ना कि उस पर जिसकी संभावना ज्यादा है। एक बार फिर यही उदाहरण लेते हैं। अगर आप 5 लाल कारें जाती देखें तो आपको ये लगेगा कि अगली कार तो पीली ही होगी। लेकिन चाहे कितनी भी कारें गुजर जाएं अगली कार फिर से लाल रंग की हो सकती है। हम डेटा याद रखकर ये बात समझ भी सकते हैं। पर इसकी जगह हमारा फोकस इस बात पर है जो हम देखना चाहते हैं। यानि इतनी सारी लाल गाड़ियों के बाद एक पीली गाड़ी।
डेटा के साथ जुड़ी बाकी गल्तियों में ये एक बहुत कॉमन गल्ती है। यहां जरा गणित की भाषा में बात करनी पड़ेगी तो आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि हर चीज घटते हुए एक एवरेज पर जाती है। यानि हर तरह की सिचुएशन के लिए कोई एवरेज रिजल्ट जरूर होगा और इसमें कुछ बदलाव भी हुए तो वो उस एवरेज रिजल्ट के आसपास ही रहेंगे। जैसे कोई फुटबॉलर एक महीने में एवरेज 5 गोल करता है। अब किसी महीने उसने 10 गोल कर दिए। उसका कोच खुशी से पागल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर वो फिर साल भर हर महीने 5 गोल ही करता रहे तो उसे कोच की डांट पड़नी तय है। पर ऊपर बताए नियम के हिसाब से ये ठीक है क्योंकि वो तो अपनी एवरेज परफार्मेंस पर वापस ही लौट रहा है।
Past imperfect: हम चल रही घटनाओं से ज्यादा बीती बातों से सीखते हैं।
हमारा दिमाग किसी अनुभव को सीधे सीधे एक लाइन में याद नहीं रखता। ये समझ लीजिए कि हमारे पास मेमोरी के दो शेल्फ होते हैं। ये दोनों किसी सिचुएशन को अलग तरह से याद रखते हैं। पहली है experiencing self जो ये रिकॉर्ड रखती है कि हम इस पल क्या महसूस कर रहे हैं। यानि इस घटना से आपको कैसा लग रहा है। दूसरी है remembering self जो इस पल के बीत जाने के बाद का हिसाब रखती है। यानि इस घटना से आपको कैसा लगा? Experiencing self किसी भी घटना की ज्यादा जानकारी रखती है क्योंकि किसी घटना के दौरान होने वाली फीलिंग्स पूरी तरह सही होती हैं। लेकिन remembering self इतनी सही नहीं हो सकती क्योंकि ये घटना के हो जाने के बाद हमारे दिमाग में रजिस्टर होती है। हालांकि जब मेमोरी की बात आए तो यही ऊपर रहती है।
हमारी remembering self के डॉमिनेट करने की भी अपनी वजह है। एक है duration neglect जहां हम किसी घटना में लगे कुल समय को नजरअंदाज करके उससे बनी memory को ऊपर रख देते हैं। दूसरी है peak-end rule जहां हम किसी घटना के आखिरी हिस्से को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। Colonoscopy करा रहे लोगों के दो ग्रुप बनाकर स्टडी की गई। एक ग्रुप में लंबे समय तक ये टेस्ट जारी रखा गया यानि इनको लंबे समय तक दर्द से गुजरना पड़ा जबकि दूसरे ग्रुप में टेस्ट कम समय के लिए किया गया पर यहां आखिर में दर्द ज्यादा हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि जिस ग्रुप का टेस्ट लंबे समय तक चला यानि जिन्होंने ज्यादा देर तक दर्द झेला वो ज्यादा परेशान हुए तो आप गलत हैं। टेस्ट के दौरान लंबा समय लगाने वाले मरीजों से जब उनकी हालत के बारे में पूछा गया तो उनकी experiencing self ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन टेस्ट खत्म हो जाने के बाद remembering self ने बागडोर संभाल ली तो अब वो मरीज जिनका टेस्ट कम समय के लिए हुआ था उन्होंने कहा कि वो ज्यादा परेशान हुए। ये उदाहरण duration neglect, peak-end rule और faulty memories को बड़ी अच्छी तरह समझाता है।
Mind over matter: अपने दिमाग का फोकस बदलकर हम अपनी सोच और बर्ताव में काफी बदलाव ला सकते हैं।
हमारा दिमाग कितनी एनर्जी की खपत करेगा ये इस पर निर्भर करता है कि ये क्या काम कर रहा है। कोई ऐसा काम जहां दिमाग को ज्यादा चलाने या फोकस की जरूरत नहीं होती वहां इसे बड़ी आसानी रहती है। जैसे सब्जी काटना। ये काम आप टीवी देखते और फोन पर बातें करते हुए भी कर लेंगे। इसे हम cognitive ease कहते हैं। यहां एनर्जी लेवल में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। लेकिन किसी ऐसी जगह जहां दिमाग की कसरत हो जाए या अटेंशन की जरूरत पड़े वहां दिमाग एनर्जी खर्च करता है और थकने लगता है। पहली सिचुएशन को cognitive ease कहा जाता है और दूसरी को cognitive strain. अब इन दोनों तरह की सिचुएशन में हमारे बर्ताव पर भी अलग तरह से असर पड़ता है। पहली सिचुएशन में हमारे दिमाग की कमान सिस्टम 1 के पास रहती है और सिस्टम 2 जो कि लॉजिक लगाने और एनर्जी की खपत करने वाला सिस्टम है वो धीमा पड़ जाता है। यानि इस वक्त हम ज्यादा intuitive, creative और खुश होते हैं पर यहां हम गल्तियां भी ज्यादा करते हैं। जबकि cognitive strain वाली सिचुएशन में हमारी अवेयरनेस ज्यादा रहती है और इसलिए सिस्टम 2 कमान संभाल लेता है। ये सिस्टम 1 के मुकाबले किसी भी चीज को डबल चेक करके काम करता है। इसलिए भले ही हमारी क्रिएटिविटी कम रह जाए पर हम गल्तियां भी कम करते हैं।
लेकिन हम कुछ जगहों पर तो कोशिश करके दिमाग की एनर्जी खपत को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको cognitive ease पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसका एक तरीका है कि कोई जानकारी, डेटा या नॉलेज आप खुद को बार बार देते रहें। ऐसा करने पर हमें कोई बात ना सिर्फ ज्यादा अच्छी तरह याद हो जाती है बल्कि हम पर ज्यादा असर भी डालती है। असल में ह्यूमन ब्रेन का इवॉल्यूशन इस तरह हुआ है कि एक ही बात या घटना से बार बार गुजरने पर हम उसे बड़ी आसान तौर पर लेने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हमें कोई जानी पहचानी चीज दिखे तो हम बड़े relax हो जाते हैं। क्योंकि इस वक्त हम cognitive ease में रहते है। जबकि cognitive strain परेशानियों से निपटने में हमारे काम आता है। इस स्टेट में जाने के लिए हमें खुद को थोड़ा चैलेंज करने की जरूरत होती है। जैसे कोई ऐसा कागज पढ़ना जिसमें लिखाई साफ ना हो। हमारा दिमाग चौकन्ना होकर एनर्जी इकट्ठी करेगा और गल्तियां करने या हार मानने की गुंजाइश कम से कम होगी।

Taking chances: जिस तरह हमारे सामने संभावनाएं आती हैं उसके हिसाब से हम रिस्क का अंदाजा लगाते हैं।
यानि अपना फोकस थोड़ा बदलकर या सवाल को देखने का नजरिया बदलकर हम इनसे निपटने का तरीका बदल सकते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें लगता है कि अगर रिस्क का कोई डेटा मिल जाए तो लोग उससे बचने का एक ही तरीका अपनाएंगे। लेकिन ये बात पूरी तरह सही साबित नहीं होती। इससे जुड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे मिस्टर जोन्स नाम दिया गया। अब साइकिएट्रिस्ट के दो ग्रुप बनाकर उनसे पूछा गया कि क्या जोन्स नाम के मरीज को छुट्टी दी जा सकती है? एक ग्रुप को ये बताया गया कि इनके जैसे मरीजों के हाथापाई पर उतरने की संभावना 10% होती है। जबकि दूसरे ग्रुप से कहा गया कि ऐसे 100 में से दस मरीज हाथापाई पर उतर सकते हैं। पहले ग्रुप के जितने लोगों ने ऐसे मरीज को छुट्टी देने के लिए मना किया उसके दुगने लोग दूसरे ग्रुप में मना करने लगे।
हमारा दिमाग आंकड़ों से कैसे चकमा खा जाता है इसका एक और नमूना है denominator neglect जिसमें हम सीधी तरह से कही बात की जगह फैंसी तरीके से सामने रखी गई बात को ज्यादा सही मान लेते हैं। जैसे ये दो बातें देख लीजिए। ये दवाई बच्चों को फलानी बीमारी के खतरे से बचाती है लेकिन 0.001 परसेंट चांस हैं कि इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट हो। अब इसी बात को यूं कहा जाए – इस दवाई को लेने वाले हर एक लाख में से एक बच्चे को साइड इफेक्ट होने की संभावना है। अब दोनों बातों में फैक्ट के हिसाब से कोई फर्क नहीं है पर लाख जैसा शब्द सुनकर हमारा दिमाग अपनी तरफ से एक तस्वीर बना लेता है और यहां दूसरी बात सुनने वालों के दवाई से दूरी बनाने की संभावना ज्यादा है।
Not robots: हम रोबोट की तरह क्यों बन जाते हैं?
आखिर हम कोई चुनाव कैसे करते हैं? एक लंबे अरसे तक इकॉनमिस्ट ये दावा करते रहे कि इंसान पूरी तरह सोच समझकर यानि rational होकर फैसले करते हैं। इन्होंने यहां utility theory का नाम लिया। यानि इंसान ये देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा और क्या फायदा नुकसान होगा यानि सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा समझकर फैसले लिए जाते हैं। जैसे आपको आम से ज्यादा संतरे पसंद हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप आम जीतने के 10% चांस में भाग लेंगे या संतरे जीतने के 10% चांस में तो आपका जवाब संतरा ही होगा है ना? इस थ्योरी को सपोर्ट करने वालों में शिकागो स्कूल ऑफ इकॉनमिक्स और वहां के स्कॉलर
Milton Friedman सबसे आगे थे। इस थ्योरी का सहारा लेकर शिकागो स्कूल ने ये कहा कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग ultra- rational decision-makers होते हैं जिनको इकॉनमिस्ट रिचर्ड थेलर और लॉयर कैस सनस्टीन ने econs का नाम दिया। ये econs चीजों और वेल्थ को पूरी तरह नाप जोख कर फैसले करते हैं जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
अब जॉन और जेनी नाम के दो लोगों का उदाहरण लीजिए। इन दोनों के पास 5 मिलियन डॉलर हैं। Utility theory के हिसाब से दोनों के पास एक जितनी वेल्थ है तो दोनों को बराबर खुश रहना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मान लीजिए कि ये 5 मिलियन उन्होंने एक ही दिन किसी केसिनो में बनाए। लेकिन दिन की शुरुआत करते हुए उनके पास अलग फंड थे। जॉन के पास एक मिलियन थे और उसने चार मिलियन और जीत लिए। जबकि जेनी के पास 9 मिलियन थे और उसके पास 5 मिलियन ही बचे। यानि सीधी बात है कि एक ही सिचुएशन में utility theory अलग तरह काम करती है। आगे देखेंगे कि जब utility theory हर जगह अलग काम करती है यानि rationally अलग अलग रहती है तो हम irrational decisions भी लेते हैं।
Gut feeling: Rational decision लेते हुए भी हम पर भावनाएं हावी हो जाती हैं।
अब अगर utility theory भी काम नहीं करती तो कौन सी थ्योरी काम करती है? डेनियल ने prospect theory का नाम लिया है। ये थ्योरी, utility theory को चैलेंज करती है कि हम कभी भी पूरी तरह rational होकर नहीं सोच सकते। दो घटनाएं देखिए। पहली में आपको हजार डॉलर दिए जाते हैं। अब आपसे कहा जाता है कि आप या तो शर्तिया 500 डॉलर और लेने के लिए हां कह सकते हैं या फिर ऐसे मौके का चुनाव कर सकते हैं कि जहां और 1000 डॉलर मिलने के 50% चांस हों। अब दूसरी घटना में आपको दो हजार डॉलर दिए जाते हैं जहां या तो आपको हर हाल में 500 डॉलर वापस करने हैं या इस बात के लिए हां करनी है कि इसमें से 1000 डॉलर हारने के 50% चांस हों। अगर इंसान पूरी तरह rational होकर सोचते तो दोनों सिचुएशन में एक जैसा फैसला करते। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। पहली सिचुएशन में ज्यादातर लोग 500 डॉलर तय मिलने वाली बात पर हां करते हैं जबकि दूसरी सिचुएशन में वो चांस लेना पसंद करते हैं। Prospect theory कम से कम दो वजहों का सहारा लेकर इस घटना को अच्छी तरह समझा देती है।
ये दोनों वजह loss aversion से जुड़ी हुई हैं यानि हमारे मन में नुकसान का खतरा फायदे की खुशी से ज्यादा गहरा बैठा हुआ है। पहली वजह के मुताबिक हम चीजों को उनके reference points के हिसाब से तौलते हैं। यानि हजार या दो हजार डॉलर हमारे लिए बुनियाद हैं। अब पहली बारी पर 1500 रुपए मिलने का ख्याल जीत की तरह लगता है जबकि दूसरी बार हार की तरह। यहां कोई रीजनिंग सही तरह काम ही नहीं कर रही है। अगले नंबर पर है diminishing sensitivity principle यानि जो वेल्यू हम समझ रहे हैं वो असली वेल्यू से अलग हो सकती है। जैसे 1000 डॉलर से 900 डॉलर पर आ जाना उतना बुरा नहीं लगता जबकि 200 से 100 डॉलर पर आ जाना 50% के नुकसान की तरह बहुत बड़ा लगता है। जबकि नुकसान तो दोनों जगह 100 डॉलर का हो रहा है। इसी तरह ऊपर के उदाहरण में भी 1500 से घटकर 1000 डॉलर रह जाना 2000 से 1500 डॉलर पर आने से ज्यादा बड़ा नुकसान लगा।
False images: हमारा दिमाग ऐसी तस्वीरें बना देता है जो हमको और उलझा दें।
किसी सिचुएशन को समझने के लिए हमारा दिमाग cognitive coherence का इस्तेमाल करता है। यानि एक तस्वीर बन जाती है। जैसे हमारे दिमाग में मौसम को लेकर तरह-तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं। गर्मी का नाम लें तो चमकता हुआ सूरज और पसीना बहाते लोग नजर आने लगते हैं। सर्दी कहा जाए तो मोटे कपड़े पहने ठिठुरते हुए लोग। इसी तरह कोई फैसला लेते हुए भी हम इन तस्वीरों का सहारा लेते हैं। यानि इनको बुनियाद बना लिया जाता है। अगर आपको ये बताना हो कि गर्मी में कैसे कपड़े पहने जाते हैं तो आप गर्मी की इमेज को ध्यान में रखकर जवाब देंगे।
अब यहां परेशानी ये है कि हम इन तस्वीरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। भले ही डेटा अलग कहानी क्यों ना कहता हो। हो सकता है मौसम विभाग ने गर्मी में किसी दिन बारिश होने या रोज के मुकाबले ठंडक रहने की संभावना जताई गई हो पर आप वही हल्के कपड़े पहनकर निकल जाएं। ऐसे में आपको परेशानी होगी ही। यानि हम इन तस्वीरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हालांकि इससे बचने के तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक ही तस्वीर के भरोसे ना बैठे रहें। यानि ये बात याद करने की कोशिश करें कि पहले भी तो आप गर्मी के मौसम में बारिश में फंस गए थे। तो आप दोनों तरह की सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखें और बाहर जाते हुए छाता या रेनकोट जरूर साथ लें।